(ग) वन एवं वन्य प्राणी संसाधन – Notes (Forest and Wildlife Resources)
(ग) वन एवं वन्य प्राणी संसाधन
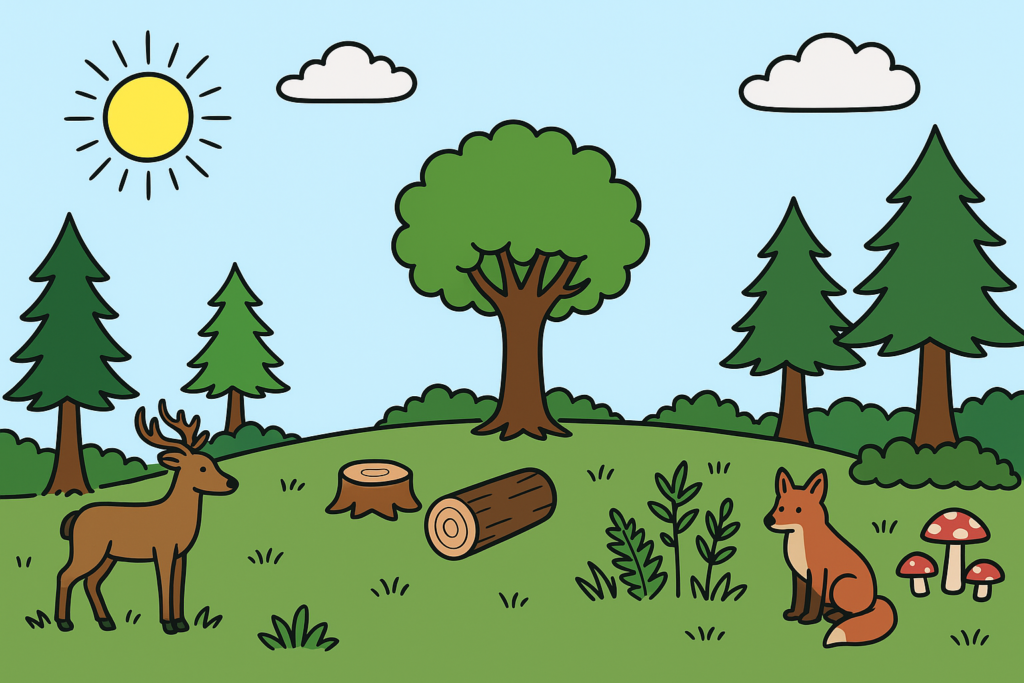
- ‘आग’ पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार है, लेकिन इसने वनों और वन्य प्राणियों को सबसे पहले प्रभावित किया।
- वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच की तरह हैं और पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं।
- वन और वन्य प्राणी खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत हैं और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
भारत में वन संसाधन
- भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन फैले हुए हैं।
- एफ० ए० ओ० की रिपोर्ट के अनुसार, 2005 में विश्व में कुल 3.952 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था।
- भारत में 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है।
वन के प्रकार –
1. अत्यंत सघन वन: 54.6 लाख हेक्टेयर, वृक्ष घनत्व 70% से अधिक।
2. सघन वन: 73.60 लाख हेक्टेयर, वृक्ष घनत्व 40-70%।
3. खुले वन: 2.59 करोड़ हेक्टेयर, वृक्ष घनत्व 10-40%।
4. झाड़ियाँ एवं अन्य वन: 2.459 करोड़ हेक्टेयर, वृक्ष घनत्व 10% से कम।
5. मैंग्रोव वन: 4.4 लाख हेक्टेयर, तटीय क्षेत्रों में।
प्रशासकीय वर्गीकरण –
(क) आरक्षित वन: वनों का 54%, बाढ़ नियंत्रण, जलवायु संतुलन के लिए।
(ख) रक्षित वन: वनों का 29%, विशेष अनुमति के तहत उपयोग।
(ग) अवर्गीकृत वन: वनों का 17%, कोई विशेष प्रतिबंध नहीं।
क्या आप जानते हैं?
- देश के कुल वन क्षेत्र का 25.11% पूर्वोत्तर राज्यों में है।
- मध्यप्रदेश में सबसे अधिक 11.22% वन क्षेत्र है।
- आदिवासी जिलों में 60.11% वन क्षेत्र पाया जाता है।
बिहार की स्थिति
- बिहार में मात्र 7.1% वन क्षेत्र है।
- पश्चिमी चम्पारण, मुंगेर, जमुई, गया, और रोहतास जिलों में वनों की स्थिति बेहतर है।
वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण
वन संसाधनों का ह्रास
- उपनिवेश काल में रेलमार्ग और सड़कों के निर्माण से वनों का विदोहन आरंभ।
- स्वतंत्रता के बाद विकास परियोजनाओं और मानव हस्तक्षेप ने स्थिति को और बिगाड़ा।
- 20वीं सदी में 24% भू-भाग पर वन थे, जो 21वीं सदी के आरंभ तक घटकर 19% रह गए।
- कारण: मानवीय हस्तक्षेप, कृषि विस्तार, पशुचारण, खनन, और औद्योगिक विकास।
विशेष उदाहरण
- झूम खेती: पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की क्षति का बड़ा कारण।
- नदी घाटी परियोजनाएं: 1952 से अब तक 5000 वर्ग किमी वन नष्ट।
- खनन: पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व डोलोमाइट खनन से प्रभावित।
- वनों का एकल रोपण: सागवान और चीड़ जैसे वृक्षारोपण से अन्य प्रजातियों का नाश।
हिमालय यव संकट
- औषधीय पौधा जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में होता है।
- अत्यधिक निष्कासन से हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में हजारों पेड़ विलुप्त।
वन्य जीवों का ह्रास
- आवास क्षेत्र का अतिक्रमण और मानवीय गतिविधियों का बढ़ता दबाव।
- प्रदूषण: पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा, वायु और जल प्रदूषण से वन्य जीवन पर असर।
- शिकार और वन्य जीवों की तस्करी: चीन तस्करी का मुख्य केंद्र।
- वर्तमान में 744 प्रजातियां विलुप्त और 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर।
मुख्य संकटग्रस्त प्रजातियां
- कृष्णा सार, भेड़िया, गेंडा, गिर सिंह, लाल पांडा, श्वेत सारस, पर्वतीय बटेर।
संरक्षण के ऐतिहासिक प्रयास
- सम्राट अशोक ने शायद विश्व में सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध और संरक्षण नियम लागू किया।
- मुगल शासन में बाबर और जहांगीर ने संरक्षण पर बल दिया।
- अमृता देवी आंदोलन: अमृता देवी ने राजस्थान में विश्नोई समुदाय के साथ मिलकर वनों की कटाई का विरोध किया।
क्या आप जानते हैं?
- भारत में 81,000 वन्य प्राणी उपजातियां और 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं।
- 100 से अधिक पौधों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में होता है।
वर्तमान समय में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण :
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास
- भारत में संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची बनाने का कार्य 1970 में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (BSI) और वन अनुसंधान संस्थान (FRI) द्वारा किया गया।
- इनकी सूची को ‘रेड डेटा बुक’ और असाधारण पौधों को ‘ग्रीन बुक’ कहा गया।
- रेड डेटा बुक:
- संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान और संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करती है।
अन्तराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ (IUCN – International Union for Conservation of Nature) या विश्व संरक्षण संघ (World Conservation Union):
संकटग्रस्त प्रजातियों को श्रेणियों में विभाजित करती है:-
1. सामान्य जातियाँ (Common species):
- ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या पर्याप्त होती है और इनकी अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं होता।
- उदाहरण:- साल, चीड़, कृतन्क (रोडेंटस)।
2. संकटग्रस्त जातियाँ (Endangered species):
- वे जातियाँ जो गंभीर खतरों का सामना कर रही हैं और जिनकी संख्या तेजी से घट रही है।
- यदि इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो इनके विलुप्त होने का खतरा है।
- उदाहरण:- काला हिरण, गेंडा, संगाई (मणिपुरी हिरण)।
3. सुभेद्य जातियाँ (Vulnerable species):
- ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है, लेकिन यह अभी संकटग्रस्त की श्रेणी में नहीं हैं।
- यदि इनपर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती हैं।
- उदाहरण:- गंगा की डॉल्फिन, नीली भेड़, एशियाई हाथी।
4. दुर्लभ जातियाँ (Rare species):
- ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम है और ये विशेष क्षेत्रों तक सीमित हैं।
- यदि इन्हें प्रभावित करने वाले कारण नहीं बदले गए तो ये संकटग्रस्त हो सकती हैं।
- उदाहरण:- हिमालयी योद्धा पौधा, लाल पांडा।
5. स्थानिक जातियाँ (Endemic species):
- ये जातियाँ केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं और अन्यत्र कहीं नहीं मिलतीं।
- उदाहरण:- अंडमानी जंगली सुअर, निकोबारी कबूतर।
6. लुप्त जातियाँ (Extinct species):
- वे जातियाँ जो अब उनके प्राकृतिक आवासों में नहीं पाई जातीं और संभवतः पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं।
- उदाहरण:- एशियाई चीता, डोडो पक्षी।
भारत में संरक्षण प्रयास
- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय:
- अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम चला रहा है।
संरक्षित क्षेत्र
राष्ट्रीय उद्यान (National Parks):
- बाहरी हस्तक्षेप रहित क्षेत्र।
- उद्देश्य:- वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना।
- भारत में राष्ट्रीय उद्यान:- 85।
अभ्यारण्य (Sanctuaries):
- सुरक्षित क्षेत्र जहाँ सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति।
- भारत में अभ्यारण्य:- 448।
- उदाहरण:- बिहार में काँवर झील, कुशेश्वर।
जैवमंडल क्षेत्र (Biosphere Reserves):
- जैव विविधता और अनुवांशिकी संरक्षण।
- विश्व में जैवमंडल क्षेत्र:- 243।
- भारत में:- 14।
महत्त्वपूर्ण संगठन
- WWF (World Wide Fund for Nature):
- संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय भूमिका।
संरक्षण के दो दृष्टिकोण
1. इन सीटू (in situ) संरक्षण:
- प्राकृतिक आवास में संरक्षण।
- राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल और अभ्यारण्य।
2. एक्स सीटू (Ex situ) संरक्षण:
- कृत्रिम आवासीय संरक्षण।
- चिड़ियाघर, प्रजनन केंद्र।
राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्यों और जैवमंडल क्षेत्रों की सूची
- भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2004-05 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्यों और जैवमंडल क्षेत्रों की सूची महत्वपूर्ण है।
- इन क्षेत्रों में संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रजनन केंद्र
- कुछ प्रजातियाँ जिनकी प्रजनन दर कम हो जाती है, संकटग्रस्त सूची में शामिल हो जाती हैं।
- मध्य प्रदेश में घड़ियालों के लिए मुरैना में प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया।
- उड़ीसा के नंदनकानन में उजले बाघों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है।
शिकार पर रोक
- शिकार और वन्य जीवों का दोहन वन्य जीवों के नुकसान का एक प्रमुख कारण है।
- हालांकि शिकार करना कानूनी रूप से वर्जित है, फिर भी काला बाजारी और तस्करी के कारण यह समस्या बनी रहती है।
- बिहार के दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान अभयारण्य में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं।
- यहां एक वॉच टावर का निर्माण भी किया गया है।
जैव अपहरण की समस्या
- जैव अपहरण (Bio Piracy) वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की जैव संपदा, जैसे पौधों और जीवों के अनुवांशिक गुणों का उपयोग बिना अनुमति के किया जाता है।
- जैव अपहरण विकासशील देशों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। उदाहरण के तौर पर, अमेरिका ने बासमती चावल के समान जर्म प्लाज्म का उपयोग किया है।
- इससे संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और हॉट स्पॉट्स चिह्नित किए जा रहे हैं।
- हॉट स्पॉट्स: वैसे क्षेत्र जो जैव विविधता में अत्यधिक समृद्ध होते हैं।
बाघ परियोजना (Project Tiger)
- बाघों की संख्या में भारी गिरावट आई थी, 1973 में बाघों की संख्या 5500 से घटकर 1827 रह गई थी।
- बाघों का शिकार, व्यापार, और उनके आवासों का नुकसान इसके प्रमुख कारण थे।
- 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई, जो विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है।
- 1985 में बाघों की संख्या 4002 और 1989 में 4334 हो गई।
- भारत में 27 बाघ रिजर्व हैं, जो लगभग 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं।
- प्रमुख बाघ रिजर्व में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (उत्तरांचल), सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल), बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश), सारिस्का वन्य जीव पशुविहार (राजस्थान), मानस बाघ रिजर्व (असम), और पेरियार बाघ रिजर्व (केरल) शामिल हैं।
क्या आप जानते हैं?
- कैमरून के बोरोरो जनजाति के लोग शेरों द्वारा किए गए शिकार पर धावा बोलते हैं, जिससे शेरों की संख्या में कमी आती है। इसे ‘क्लेप्टोपैरासाईटिज्म’ कहा जाता है।
समुदाय और वन संरक्षण
समुदाय का वन्य जीव संरक्षण में योगदान
- भारत के कई क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वन्य जीवों के आवास स्थलों के संरक्षण में कार्यरत हैं।
- राजस्थान के सरिस्का बाघ रिजर्व में गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत खनन कार्य रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- अलवर जिले के 5 गाँवों ने 1,200 हेक्टेयर वन भूमि ‘भैरोंदेव डाकव’ विहार चोरी घोषित कर दी है, जो शिकार को वर्जित करता है और बाहरी लोगों से वन्य जीवन की रक्षा करता है।
आदिवासी समुदाय और वन संरक्षण
- आदिवासी लोग अपनी जीवनशैली के लिए वन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं।
- इनका वन्य जीवों और पेड़-पौधों से गहरा भावनात्मक और आत्मीय संबंध होता है।
- प्रजनन काल में ये मादा वन पशुओं का शिकार नहीं करते और वन संसाधनों का चक्रीय पद्धति से उपयोग करते हैं।
- वे वृक्षारोपण और संरक्षण का कार्य समय-समय पर करते हैं, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में स्वाभाविक वन संरक्षण होता है।
चिपको आंदोलन
- चिपको आंदोलन 1972 में उत्तर प्रदेश के टेहरी-गढ़वाल क्षेत्र में शुरू हुआ था, जिसमें लोग ठेकेदारों द्वारा काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें अपनी बाहों में लपेटकर उनकी रक्षा करते थे।
- इस आंदोलन ने पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित किया और सामुदायिक वनीकरण के महत्व को साबित किया।
संयुक्त वन प्रबंधन
- 1988 में उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत हुई।
- इस योजना में वन विभाग और ग्रामीण समुदाय मिलकर क्षरित वनों का प्रबंधन और पुनर्निर्माण करते हैं।
जैन और बौद्ध धर्म और वन संरक्षण
- जैन और बौद्ध धर्म अहिंसा पर आधारित हैं और इन धर्मों के अनुयायी वन्य जीवन के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।
- महात्मा बुद्ध ने पेड़ों को विशेष रूप से उदार और दयालु जीवधारी बताया था जो किसी मांग के बिना अपनी जीवन क्रियाएँ अन्य जीवों के लाभ के लिए करते हैं।
वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान
अंतर्राष्ट्रीय नियम
- वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समझौते और कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे:
- अफ्रीकी कनवेंशन (1968)
- Ramsar Convention (1971)
- विश्व प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण अधिनियम (1972)
राष्ट्रीय कानून
- भारत का संविधान वन्य जीवन और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रावधान करता है, जैसे अनुच्छेद 47, 48 और 51A (जी)।
- भारतीय वन्य जीवन बोर्ड 1952 में स्थापित हुआ था, जिससे वन्य जीवों के संरक्षण में सरकार का ध्यान केंद्रित हुआ।
- 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुए, जिनके अंतर्गत पक्षियों और जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया।
- जैव विविधता अधिनियम (2002) के तहत जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थानीय, जिला और राज्य स्तर पर समितियाँ गठित करने का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय स्तर पर बाघ और मयूर को राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है।
जैव विविधता का महत्व
- राष्ट्र के स्वस्थ जैव मंडल और जैविक उद्योग के लिए समृद्ध जैव विविधता अनिवार्य है।
- जैव विविधता हमें भोजन, औषधियाँ, रेशे, रबर और लकड़ियों का साधन प्रदान करती है।
- यह सूक्ष्म जीवों के रूप में उद्योगों के लिए बहुमूल्य उत्पाद तैयार करने में भी सहायक है।
- जैव विविधता हमें पारिस्थितिकीय सेवाएँ जैसे जल, वायु, और मृदा संरक्षण मुफ्त में प्रदान करती है।
आधुनिक कृषि में जैव विविधता का उपयोग
- आधुनिक कृषि जैव विविधता का तीन प्रमुख तरीकों से उपयोग करती है:-
- नवीन फसल के साधन के रूप में
- अच्छे प्रकार के नस्ल के लिए सामग्री के रूप में
- नए जैव विनाश और पीड़ानाशी के रूप में
- मानव का भोजन मुख्यतः जैविक संसार से प्राप्त होता है, और 85% भोजन 20 से कम पौधों की प्रजातियों से उत्पन्न होता है।
- जंगली प्रजातियाँ कृषि में सुधार के लिए काम आती हैं, जैसे रोग रोधी गुण और अधिक उपज देने वाली घरेलू प्रजातियाँ।
- एशिया में धान की खेती का चार प्रमुख रोगों से संरक्षण एक अकेला जंगली भारती चावल प्रजाति ओर्जिया निवारा (Orzya nivara) द्वारा किया जाता है।
औषधीय उपयोग में जैव विविधता
- जैव विविधता से कई औषधियाँ और उपचार तैयार होते हैं:-
- मार्फीन (Papaver somniferum) – दर्द निवारक
- क्यूनाईन (Chinchona ledgeriana) – मलेरिया के लिए
- टेक्सोल (Taxus baccata) – कैंसर रोधी
- लगभग 25% भैषज्य दवाइयाँ 120 पौधीय प्रजातियों से तैयार होती हैं।
सच्ची कहानी: ‘आरोग्यपाचा’ और कानी आदिवासी समुदाय
- दिसम्बर 1987 में, TBGRI संस्था के वैज्ञानिकों ने केरल के पश्चिमी घाट में कानी आदिवासियों के साथ मिलकर जैविक अभियान चलाया।
- आदिवासी समुदाय के लोग एक फल खा रहे थे, जिसे खाने से उन्हें अधिक ऊर्जा मिली।
- वैज्ञानिकों ने इसे खाकर अनुभव किया और इसके बारे में जानकारी प्राप्त की।
- यह फल ‘आरोग्यपाचा’ नामक पौधे से उत्पन्न होता है, जो तनाव रोधक और अन्य लाभकारी गुणों से भरपूर था।
- इस पौधे के मिश्रण से एक औषधि तैयार की गई, जिसका नाम ‘जीवानी’ रखा गया।
- TBGRI ने इसे एक प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस दिया, और कानी समुदाय को आधी रॉयल्टी दी, जिससे उन्होंने अपने कल्याण के लिए ट्रस्ट स्थापित किया।
- इस कहानी ने यह सिद्ध किया कि एक पौधे ने कैसे स्थानीय समुदाय को लाभ पहुँचाया।
आयुर्वेद और जैव विविधता
- आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयाँ पौधों, जन्तुओं और खनिजों से बनाई जाती हैं।
- आयुर्वेद की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और यह भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक प्रमुख पद्धति है।
- चरक, आयुर्वेद के जनक ने पादप, जन्तु और खनिजों का उपयोग रोग उपचार के लिए किया था।
